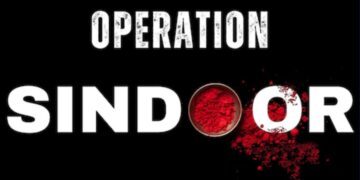प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जाति आधारित गणना कराने की मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCPA) की बैठक के दौरान लिया. इसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी ने की था. बता दें कि आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होगी. अब तक की 7 जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों की गणना होती थी. हमारे संविधान में अभी तक केवल SC और ST की गिनती करने का ही प्रावधान है, लेकिन इस बार OBC को भी इस दायरे में शामिल किया जाएगा. अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)की भी गिनती होगी.
जातिगत जनगणना का असर हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होने वाला है. जातिगत जनगणना के आंकडे आने के बाद आरक्षण को लेकर बहस छिड़ सकती है. अगर बात पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां जातियों का जमावड़ा हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रहा है. आइए जानें देश में जातिगत जनगणना होने से हिमाचल प्रदेश पर क्या असर देखने को मिलेगा.
हिमाचल का जातीय समीकरण
मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के बाद, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसका असर पड़ेगा. देश में इसके संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, अपनी खास सामाजिक संरचना के साथ, इस ऐतिहासिक निर्णय के परिणामों से अछूता नहीं रहेगा. जातिगत जनगणना के आंकड़े राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में विभिन्न जातियों का एक विशिष्ट मिश्रण है. राजपूत यहां एक प्रभावशाली समुदाय है. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों की भी राज्य की जनसंख्या में एक उल्लेखनीय हिस्सेदारी है. इन सभी समुदायों के अपने सामाजिक रीति-रिवाज, आर्थिक स्थितियां और राजनीतिक प्रभाव रहे हैं.
जनसंख्या के आधार पर हिमाचल का जातिगत समीकरण इस प्रकार है-
साल 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 68,64,602 है. इनमें 34,81,873 पुरुष और 33,82,729 महिलाएं हैं.
हिमाचल में 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या सवर्ण (General) है. जिसमें सबसे ज्यादा 32.72 प्रतिशत राजपूत हैं और 18 प्रतिशत ब्राह्मणों की जनसंख्या है. इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) 25.22% और अनुसूचित जनजाति (ST) की जनसंख्या 5.71% है. हिमाचल प्रदेश में ओबीसी (OBC) 13.52 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 4.83 प्रतिशत हैं.
(भारत में साल 2011 की जनगणना के आधार पर )
जाति जनसंख्या (प्रतिशत में)
सामान्य वर्ग 50.72%
अनुसूचित जाति 25.22%
अनुसूचित जनजाति 5.71%
ओबीसी 13.52%
अल्पसंख्यक 4.83%
साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, जिसकी कुल जनसंख्या 1,507,223 है. वहीं, सबसे कम जनसंख्या लाहौल-स्पीति जिले की है, जिसकी कुल जनसंख्या केवल 31,528 है. हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.57 प्रतिशत है. सबसे अधिक शहरी जनसंख्या शिमला में है और सबसे कम लाहौल-स्पीति में है. हिमाचल की 90 प्रतिशत पॉपुलेशन गांव में बाकी की 10 प्रतिशत शहर में रहती है.
सरल भाषा में समझें क्या है जातिगत जनगणना?
जाति जनगणना शब्द, तीन शब्दों (जाति+ जन+ गणना) से मिलकर बना है. जिसमें जन का अर्थ है लोग और गणना का मतलब है गिनती करना. आसान भाषा में कहें तो, लोगों से जाति पूछकर उनकी गिनती करना. इसे करने का उद्देश्य ये पता लगाना है कि देश और स्थान विशेष में किस जाति के कितने लोग रहते हैं. जातिगत जनगणना से देश में निवास करने वाले SC/ST और OBC लोगों की जानकारी तो इकट्ठा होगी ही, इसके साथ ही उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का पता चलेगा.
पहले जनगणना में केवल SC-ST जातियों की गिनती होती है, लेकिन अब जाति जनगणना मं OBC जाति को भी शामिल कर दिया गया है.
जातिगत जनगणना का इतिहास और इसकी जरूरत
देश में सबसे पहली बार जनगणना 1972 में ब्रिटिश काल में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी. हालांकि ये एक शुरुआती प्रयोग था, जिसे पूर्ण जनगणना नहीं माना जाता. इसके बाद पहली पूर्ण जनगणना साल 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पर की गई थी. इसमें पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी जारी किया गया था. इसके बाद से 10 साल के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती है.
साल 1881-1931 तक जातिगत जनगणना करवाई गई. इसके बाद इसे स्वतंत्र हुए भारत में बंद कर दिया गया. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में साल 2011 की जनगणना में जातिगत जनगणना हुई थी मगर इसके आंकडे़ ऑफिशियली जारी नहीं किए गए थे.
संविधान में जनगणना को लेकर क्या हैं प्रावधान?
भारतीय संविधान में जनगणना कराने को लेकर डीटेल में उल्लेख किया गया है. बता दें कि संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत जनगणना संघ सूचि का विषय है. यह संविधान की सातवीं अनुसूची के 69 नंबर में सूचीबद्ध है. यानि जनगणना कराने और उससे संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है. जबकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है. इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूचि में जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं.
जातिगत जनगणना की जरूरत
जातिगत जनगणना हर क्षेत्र की जातियों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
सरकार को जरूरतमंद जातियों के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में आसानी होगी.
जातिगत जनगणना से यह पता चल पाएगा कि अभी जो आरक्षण चल रहा है, वह ठीक है या नहीं. इससे यह भी मालूम होगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और वे सामाजिक और आर्थिक रूप से कितने पीछे हैं.
इससे सरकार को यह पता चलेगा कि अलग-अलग जातियों के कितने लोग हैं, वे कितने पढ़े-लिखे हैं, उनकी कमाई कैसी है और उन्हें स्वास्थ्य जैसी किन चीजों की जरूरत है.